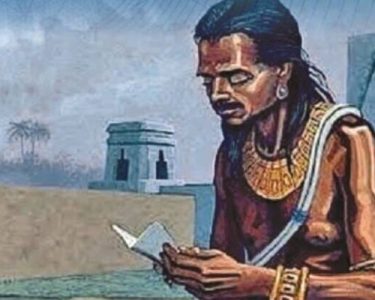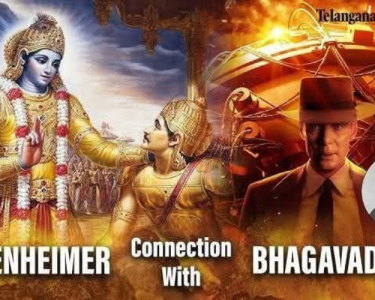प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था / ४
- प्रशांत पोळ
विजयनगर साम्राज्य में न्याय व्यवस्था यह अनेक स्तरों पर रची हुई थी। ग्राम स्तर पर निर्णय ग्राम सभा लेती थी। यह ग्राम सभा गांव के बुजुर्ग, जानकार लोग आपस में चर्चा करके तय करते थे। ग्राम सभा, साधक-बाधक और निःष्पक्ष रूप से निर्णय लेती थी। अगर यह निर्णय किसी व्यक्ति को मान्य नहीं होता था, तब वह व्यक्ति निर्णय के लिए शासकीय अधिकारी के पास जाती थी। वहां भी अगर समाधान नहीं मिला तब यह प्रकरण दंडनायक के पास जाता था। दंडनायक एक प्रकार से उसे क्षेत्र का न्यायालयीन प्रमुख होता था। दंडनायक के पास भी समाधान नहीं हुआ तो, महाप्रधानी के पास जाते थे। महाप्रधानी, दरबार में प्रकरण को (केस को) चलाते थे। उनसे भी उचित निर्णय नहीं हुआ तो फिर्यादी राजा तक जा सकता था। राजा, मुख्य न्यायाधीश होता था। उसका धर्मशास्त्र का अध्ययन रहता था। और राजा का निर्णय अंतिम होता था। दोनों पक्षों को उसे स्वीकारना अनिवार्य होता था।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के प्रारंभिक काल में, जब बुक्का राय राज्य के प्रमुख थे, तब सन 1368 में जैन और वैष्णव पंथों में विवाद हुआ। किसी भी न्यायालय स्तर पर इस विवाद का निराकरण नहीं हो पाया। इसलिए यह विवाद बुक्का राय के सामने आया। राजा ने पूरा मामला संज्ञान में लिया। धर्मशास्त्र का आधार लिया,और अपना न्याय किया। यह न्याय दोनों पक्षों को सहर्ष मान्य हुआ।और दोनों पंथों के बीच का विवाद समाप्त हुआ।
सन 1406 में दो गांवों में हुए विवाद के संदर्भ में जो कागज मिले हैं, उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। चिंगल पेट जिले के दो गांवों में पानी के कारण संघर्ष खड़ा हुआ। अंत में यह मामला महाप्रधानी के पास आया। उन्होंने उस प्रकरण को सफलता से सुलझाया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं।
सन 1446 में देवराया (द्वितीय), विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, तब ‘पडाईवीडू’ राज्य ने न्याय व्यवस्था में संशोधन (amendment) किया। इस राज्य ने कन्या शुल्क, अर्थात दहेज को गैर कानूनी बनाया। और उसके अनुसार कानून लागू किया। इसका अर्थ है, उस समय, किसी एक स्तर तक, साम्राज्य के मांडलिक राज्यों को सामान्य जनों के कल्याण के लिए, कानून में बदलाव करने की अनुमति थी।
सन 1532 में अच्युतदेव राय राजा थे। उस समय विजयनगर साम्राज्य के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा गांव था, ‘कवतला’। इस गांव के नागरिक, शासकीय अधिकारियों के जुल्म से, उन्होंने लगाए हुए जुल्मी करों के कारण और उन पर जो अन्याय हो रहा था उससे त्रस्त हो गए थे। इसी कारण से उन्होंने ‘कवतला’ छोड़कर ‘मसावेया’ इस गांव में स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। अन्याय के कारण हुए इस स्थानांतरण का समाचार सुनकर, उसे क्षेत्र के महामंडलेश्वर ‘सलकाया देवासिका तिरुमला राजा महा’ ने इस घटना की सुओ मोटो (Suo Moto) अर्थात, स्वयं आगे जाकर, जानकारी ली। वह उन स्थानांतरित नागरिकों से आकर मिले। उनकी शिकायतें सुनी। जुल्म ढाने वाले, अन्याय करनेवाले अधिकारियोंपर पर मुकदमा चलाया। और उन सब स्थानांतरित नागरिकों को कवतला यह उनके स्वयं के गांव में पुनः स्थापित किया।
व्यक्तिगत स्तर से लेकर राजनीति के स्तर तक, अनेक दीवानी और फौजदारी मामले, विजयनगर साम्राज्य के कालखंड में चलाए गए। इनमें से अधिकतम मामले इन ऐतिहासिक कागजों में मिलते हैं। इन सब मामलों में ‘धर्मशास्त्र’ की अर्थात, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, मिताक्षर आदि ग्रंथोंकी सहायता ली हुई है। इसलिए निर्णय निष्पक्ष रूप से, न्याय पूर्ण पद्धति से होते थे। यह निर्णय सामान्य जनता को मान्य होते थे। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य में कानून व्यवस्था उच्च स्तर की थी। कहीं भी असंतोष नहीं था। ऐसा अनेक तत्कालीन विदेशी यात्रियों ने लिखकर रखा है।
आगे चलकर, महाराष्ट्र में 6 जून 1674 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तब उन्होंने राजकाज चलाने के लिए अष्टप्रधानों की नियुक्ति की। इन अष्टप्रधानों में दो पद विशेष रूप से कायदा – कानून और परंपरा जतन करने के लिए थे।
- न्यायाधीश 2. पंडित राव
इनमें से पंडित राव यह पद प्रमुखता से धार्मिक विधि और परंपराओं की व्यवस्था देखने के लिए था। किंतु पंडित राव के पद पर रहने वाली व्यक्ति, धार्मिक और पारंपरिक विवादों में न्याय दान का भी काम करती थी। स्वराज के प्रथम पंडित राव थे – मोरेश्वर पंडित।
निराजी पंत रावजी यह हिंदवी स्वराज्य के पहले सर न्यायाधीश थे। दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में निर्णय देकर जनता को न्याय दिलाने का काम करते थे।
निराजी रावजी के ही पुत्र प्रहलाद निराजी यह छत्रपति संभाजी महाराज के समय, अर्थात 1682 से 1688 इस कालखंड में, स्वराज्य के मुख्य न्यायाधीश थे। यह कालखंड अस्थिरता का और युद्ध का कालखंड था। फिर भी इस कालखंड में न्याय दान का कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहा था।
पेशवाओं के कार्यकाल में भी न्याय दान की पद्धति सुव्यवस्थित थी। ग्राम स्तर पर ‘गोतसभा’ या ‘ग्राम सभा’ न्याय देने वाली प्रारंभिक सीढ़ि थी। सर्वोच्च स्थान पर न्यायाधीश यह पद था, जो पुणे में रहता था। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मराठाशाही स्थिर हो रही थी। तब 1709 से 1719 तक सखो विट्ठल यह मुख्य न्यायाधीश थे।
आगे चलकर, रामशास्त्री प्रभुणे 1750 में पेशवा के शास्त्री मंडल में दाखिल हुए। पुणे दरबार के न्यायाधीश इस पद पर उनकी नियुक्ति हुई। माधवराव पेशवा ने उन्हें सर न्यायाधीश नियुक्त किया। नारायण राव पेशवा की हत्या के जुर्म में उन्होंने प्रत्यक्ष रघुनाथ राव पेशवा को ही देहांत प्रायश्चित, अर्थात मृत्यु की सजा सुनायी।
कुल मिलाकर, अंग्रेजों का राज आने तक, भारत में एक व्यवस्थित दस्तावेजीकरण (Well documented) से परिपूर्ण, न्याय प्रणाली कार्यरत थी। इस न्याय व्यवस्था का आधार धर्मशास्त्र के ग्रंथ थे। यहां ‘धर्म’ यह रिलिजन के अर्थ से उपयोग नहीं होता था। इन धर्म ग्रंथो द्वारा दिए गए निर्णय सर्वमान्य होते थे। इसीलिए इस्लामी आक्रांता आने तक अपने देश में व्यवस्था के प्रति असंतोष नहीं था। क्योंकि राज्य यह ‘धर्म ‘से चलने वाला राज्य होता था।
अंग्रेजों ने उनके प्रारंभिक कालखंड में, अर्थात बंगाल पर उनके शासन स्थापित होने के बाद, न्याय देते समय हिंदू धर्म ग्रंथो का आधार लिया था। परंतु वह केवल प्रारंभ में। बाद में उन्होंने अपने कायदे – कानून चलाना प्रारंभ किया।
इंग्लैंड के जो कानून भारत में लगाए गए, उनका मुख्य आधार ‘व्यक्ति का अधिकार’ था। यह कल्पना हमारे न्याय व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत थी।भारतीय न्याय व्यवस्था का आधार यह ‘व्यक्ति का अधिकार’ नहीं था, अपितु ‘व्यक्ति का कर्तव्य’ था। प्राचीन पारंपरिक हिंदू न्याय शास्त्र में ‘व्यक्ति के अधिकार’ यह विषय ही नहीं था। संपूर्ण न्याय शास्त्र ही ‘सामान्य नागरिकों का कर्तव्य’ इस विषय पर आधारित था।
अर्थात, मूल संकल्पना ही बदल गई। इसके कारण हमारा समाज जीवन भी बदला। लोगों का न्याय मिलने वाले पद्धति को देखने का दृष्टिकोणभी बदला। और लाखों मामले, प्रलंबित अवस्था में वर्षों तक रहने लगे।
- प्रशांत पोळ
(आगामी प्रकाशित ‘भारतीय ज्ञान का खजाना – भाग २’ इस पुस्तक के अंश)