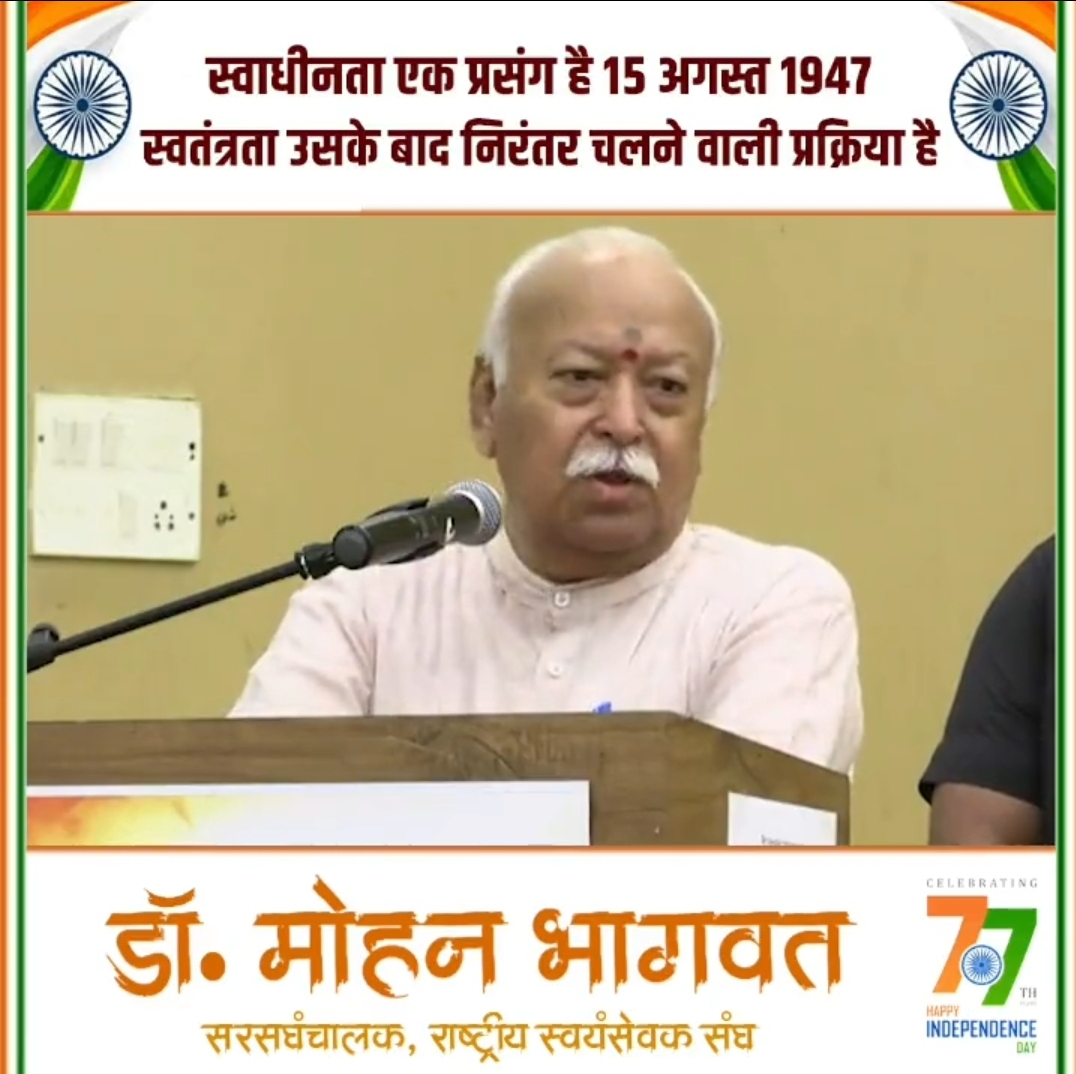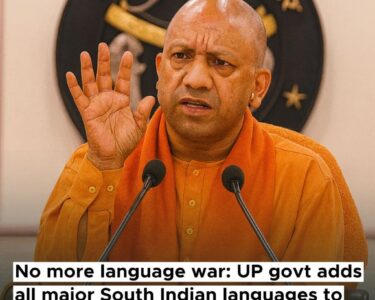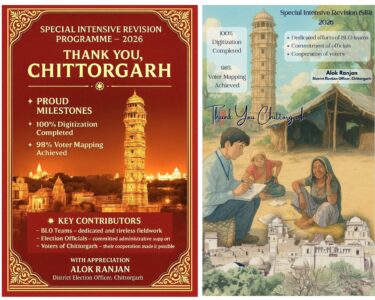20अगस्त
स्वतन्त्रता दिवस के संदर्भ में RSS के पू सरसंघ चालक द्वारा दिये गए वक्तव्य “स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक” पर आधारित लेख माला। लेख सदानन्द सप्रे जी की पुस्तक से लिया गया है। इस श्रंखला का ये 5वां लेख प्रस्तुत है।
स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक
स्वतन्त्रता नियमित चलने वाली प्रक्रिया है।- 5
आज का विषय-
समाज-निर्भर तंत्र (भौतिक उन्नति से सबंधित)
समाज की भौतिक उन्नति से संबंधित समस्त तंत्र (अर्थ-उद्योग, स्वावलंबिता-स्वदेशी, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, कृषि इत्यादि) भारत समाज-निर्भर और भारतीय चिन्तनपर आधारित होने चाहिए।
अंग्रेजों ने जानबूझकर यह संभ्रम फैलाया कि भारत में केवल आध्यात्मिक उन्नति का ही विचार किया जाता रहा है, भौतिक उन्नति का नहीं; जबकि भारत में चार सर्वमान्य पुरुषार्थों में से (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) दो पुरुषार्थ आध्यात्मिक क्षेत्र के हैं (धर्म और मोक्ष) और दो पुरुषार्थ भौतिक क्षेत्र के हैं (अर्थ और काम)। इस तरह भारतीय चिंतन में आध्यात्मिकता और भौतिकता में सुंदर समन्वय और संतुलन है जो मानवमात्र के लिए आवश्यक है। पश्चिमी चिंतन मुख्यतः भौतिकता आधारित है और इसीलिए उसपर आधारित तंत्रों के कारण आज अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, होती जा रही हैं। इन सब का समाधान भारत कर सकता है और आज के भारत के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। परन्तु इसके लिए हमें भारतीय चिंतन को पूरी तरह समझना होगा और अपने समस्त तंत्रों को उसपर आधारित बनाना होगा उसमें आवश्यक कालसुसंगत परिवर्तन करते हुए।
यह ध्यान में रखना होगा कि ‘धर्म’ याने ‘Religion’ नहीं। Oxford dictionary में भी ‘Dharma’ (धर्म) का अर्थ दिया है – ‘Eternal Law of Universe’ (ब्रह्मांड का शाश्वत नियम) और ‘Religion’ का अर्थ दिया है – ‘A particular way of worship and faith’ (पूजा-उपासना और आस्था – विश्वास की विशिष्ट पद्धति)। हम जानते ही हैं कि ब्रह्मांड में सब जगह समन्वय और संतुलन है, कहीं भी संघर्ष नहीं है। इसी कारण समूचा ब्रह्मांड (सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्धारित) नियमानुसार अनुशासन में चलता रहता है और इस तरह उसकी धारणा होती है।
[ ‘धर्म’ यह शब्द संस्कृत के धातु ‘धृ’ से निकला है; जिसका अर्थ हैं . ‘ध्रियते लोकः अनेन’ (जिसके कारण ब्रह्मांड की धारणा होती है) और ‘धरति लोकं वा’ (जो ब्रह्मांड की धारणा करता है) । ]
अन्य सभी चिंतनों के अनुसार भारतीय चिंतन में भी मानव जीवन का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। परन्तु जहाँ अन्य चिंतनों में सब सुख बाह्य वस्तुओं में है ऐसा माना जाता है, वहीं भारतीय चिंतन कहता है कि, सुख मन के अंदर है और वह व्यक्ति की चित्त-वृत्तिपर निर्भर करता है। मानव का स्वभाव ऐसा है कि एक अकेला आदमी सुखी नहीं हो सकता। वह अपने आसपास के लोगों को भी सुखी देखना चाहता है, क्योंकि उनके दुख के कारण उस के सुख में बाधा पड़ती है। इसीलिए भारत में अपने आराध्य की प्रार्थना करते समय केवल व्यक्तिगत सुख की कामना नहीं की जाती; कहा जाता है- ‘सर्वे भवन्तु सुखिन:’ (सब सुखी हों), ‘भवतु सब्ब मंगलम्’ (सभी का मंगल/कल्याण हो), ‘सरबत दा भला’ (सब का भला हो)। [ जब भी किसी का मंगल होता है, कल्याण होता है, भला होता है तब वह सुखी होता है । ]
क्या है सुखी समाज की संकल्पना कल के लेख में अर्थ एवम उद्योग सन्दर्भ में बात करेंगे।………क्रमशः