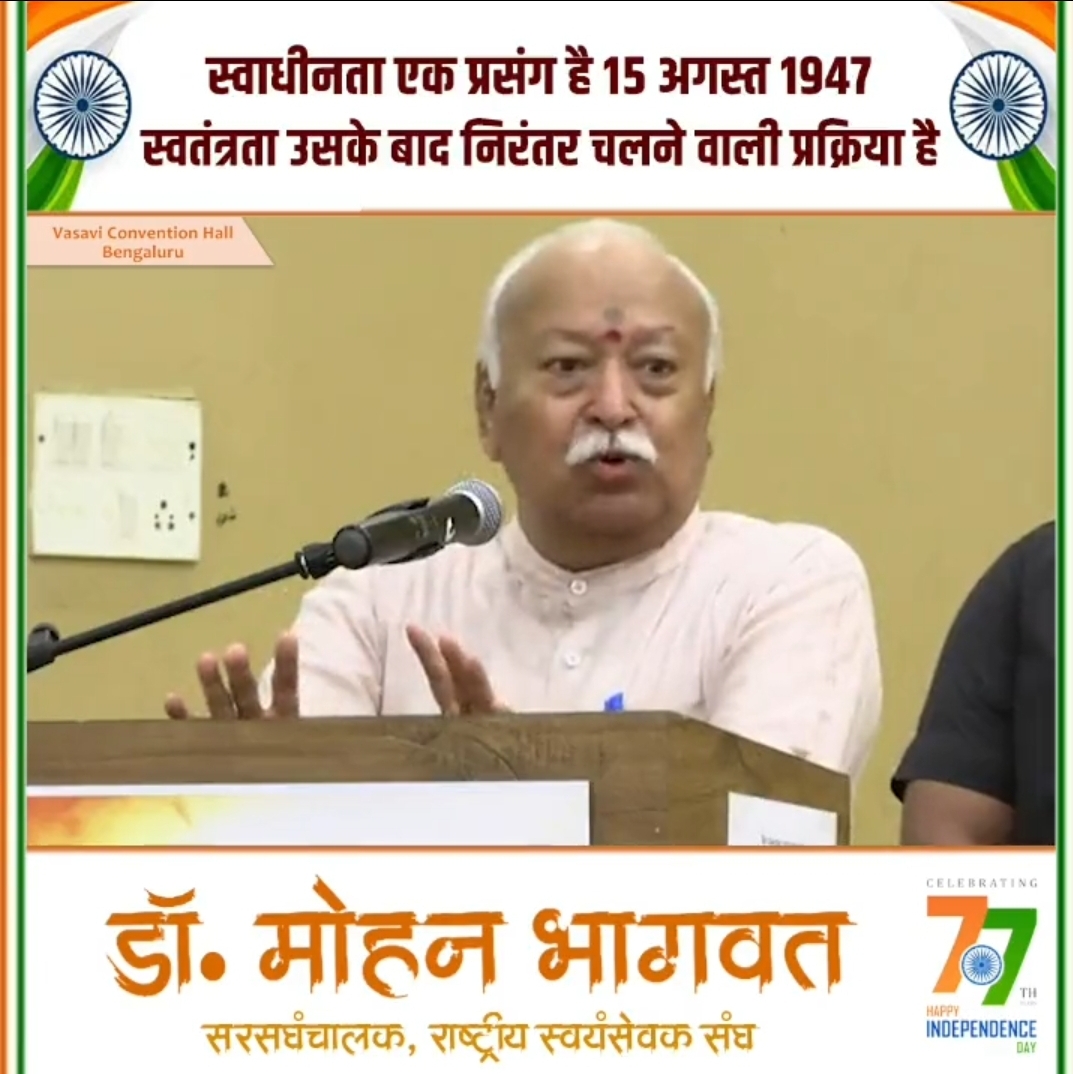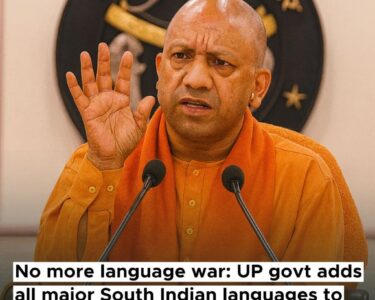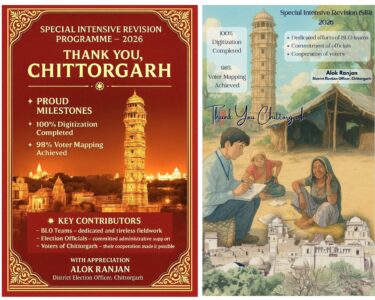21अगस्त
स्वतन्त्रता दिवस के संदर्भ में RSS के पू सरसंघ चालक द्वारा दिये गए वक्तव्य “स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक” पर आधारित लेख माला। लेख सदानन्द सप्रे जी की पुस्तक से लिया गया है। इस श्रंखला का ये छःठवां लेख प्रस्तुत है।
स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक
स्वतन्त्रता नियमित चलने वाली प्रक्रिया है।-6
आज का विषय- अर्थ एवं उद्योग
अपने यहाँ कहा जाता है कि, सुख का मूल धर्म में है और धर्म का मूल अर्थ में है (सुखस्य मूलं धर्मम्, धर्मस्य मूलं अर्थम् । ) । जब मनुष्य का जीवन धर्म के आधारपर चलता है तब उसमें समन्वय, संतुलन और अनुशासन होता है और उसके कारण ब्रह्मांड की (जिसमें समाज भी शामिल है) धारणा होती है, जिसके कारण समाज का भला होता है और वह सुखी होता है। इसीलिए कहा गया है कि सुख का मूल धर्म में है। धर्म के कारण समाज की धारणा होती है और वह सुखी होता है। परन्तु ऐसा होने के लिए अर्थ की, याने भौतिक संपदा की, आवश्यकता होती है । इसीलिए कहा गया है कि धर्म का मूल अर्थ में है।
पश्चिमी चिंतन में व्यक्ति के निजी सुख का विचार है। अतः उन की आर्थिक दृष्टि का लक्ष्य है व्यक्ति का निजी सुख, जबकि भारतीय चिंतन में सबके सुख का विचार है। अतः हमारी आर्थिक दृष्टि का लक्ष्य है – सब का सुख । दोनों ही अर्थतंत्र अपने-अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर बने हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कई मामलों में अलग-अलग हैं। अंग्रेजों के शासन के कारण अन्य तंत्रों की तरह हमारा अर्थतंत्र भी पश्चिमी चिंतन के अनुसार है। अतः भारतीय चिंतन के
आधारपर इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जाने चाहिए।
पश्चिमी चिंतन में व्यक्ति को मुख्यतः केवल शरीर ही माना जाता है। इसकी मुख्यतः तुलना में मन और बुद्धि को बहुत कम माना जाता है और आत्मा को तो उससे भी कम माना जाता है। अतः उनके चिंतन के अनुसार निजी सुख में भौतिकता का ही विचार है। भारतीय चिंतन में व्यक्ति का विचार शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इस तरह समग्रता से किया जाता है। इसलिए इसमें निजी सुख में भौतिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों ही विचार हैं। भारतीय चिंतन में सब के सुख का विचार है, अतः इसमें निजी सुख के साथ दूसरों का सुख भी आता है। दूसरों के सुख का विचार कोई व्यक्ति तभी कर सकता है, जब वह उन्हें अपना मानता है, अपने जैसा मानता है। ‘एक ही परमात्व तत्त्व सबमें है’ ऐसा विचार हो तभी यह संभव है और यही आध्यात्मिकता है। इसलिए सब के सुख में भौतिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों ही विचार हैं। इसलिए हमारा अर्थतंत्र भी ‘जियो और जीने दो’ (Live and let live) इस सोचपर आधारित होना चाहिए क्योंकि तभी सब सुखी होंगे।
भारतीय चिंतन में अर्थ और काम का विचार तो है, लेकिन वह अनियंत्रित न होकर धर्म द्वारा नियंत्रित हो ऐसा कहा गया है। (‘धर्म’ का अर्थ ‘religion’ नहीं।) इसलिए हमारे यहाँ कितना कमाया इससे महत्त्वपूर्ण है, कैसे कमाया। (धर्म-सुसंगत मार्ग से या धर्म-विरुद्ध मार्ग से ?) इसी तरह कितना कमाया इससे महत्त्वपूर्ण है, कितना बाँटा (क्योंकि बाँटने से समाज के दुःख कम होकर उस का सुख बढ़ता है जिससे समाज की धारणा अधिक अच्छी तरह होती है और धर्म का उद्देश्य है ‘समाज की धारणा करना’। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है ‘एक हाथ से कमाओ और हजार हाथों से बाँटो’।) काम की पूर्ति के लिए उपभोग करने की मनाही नहीं है, लेकिन वह धर्म द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ ‘संयमित उपभोग’, ‘त्यागपूर्वक उपभोग’ (तेन त्यक्तेन भुंजीथाः) के लिए कहा गया है। इसके लिए ‘इंद्रियनिग्रह’ आवश्यक है।
[ यद्यपि भारतीय चिन्तन में कैसे कमाया, कितना बाँटा, संयमित उपभोग इत्यादि बातें हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है। इस धन में धन कमाने को बुरा माना गया है। अपने यहाँ तो कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति ने इतना तो कमाना ही चाहिए कि गृहस्थ जीवन के आवश्यक कर्तव्य (रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और अतिथि सत्कार) पूरे किए जाने के अलावा, और अन्य विशेष दिन अच्छी तरह मनाए जा सकें तथा परिवार के लोगों की पर्व-त्यौहार
स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। यह सब करने के बाद भविष्य की दृष्टि से बचत और समाजोपयोगी काम तथा ऐसे कामों में योगदान भी उस कमाई में से होना चाहिए।
● इसमें बताई हुई अन्तिम बात ‘समाजोपयोगी काम तथा ऐसे कामों में ‘योगदान’ अच्छी तरह की जा सके इसीलिए कहा गया है कि ‘हजार हाथों से ‘बाँटो’। परन्तु यह सब किया जा सके इतना धनार्जन ‘एक हाथ से कमाओ’ के अंतर्गत किया जाना चाहिए। यह बात सरल नहीं है और इसीलिए चार पुरुषार्थों में ‘अर्थ’ भी शामिल है, केवल एक शर्त के साथ – ‘धर्म’ के नियंत्रण में ‘अर्थ ‘हो, याने कमाने का मार्ग धर्म से सुसंगत हो। ।
संयमित उपभोग के कारण स्वतः पर खर्च कम होकर बचत अधिक होती है। (कोरोना महामारी का भारत के लोगोंपर और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर सबसे कम दुष्परिणाम होने का एक प्रमुख कारण है, हमारे परिवारों का बचत करने का स्वभाव।) भारतीय अर्थचिंतन में कमाने के उपाय बताने के साथ, लौटाने (giving back) के मार्ग भी बताए जाते हैं; क्योंकि भारतीय संस्कृति में उऋण होने को बहुत महत्त्व दिया गया है और giving back वाला विचार उसी दिशा का है।
भारतीय चिंतन में आर्थिक व्यवस्था मानव केंद्रित होती है, धन केंद्रित या लाभ केंद्रित या प्रौद्योगिकी केंद्रित या साधन केंद्रित नहीं। इसलिए वह सह अस्तित्व और पारस्परिक सहयोग की भावना पर आधारित है। पश्चिमी चिंतन भी अब धीरे-धीरे इसी दिशा में आ रहा है। इसीलिए वहाँ अब ‘मानवीय चेहरेवाला विकासपथ’ (Path of developement with human face) इस तरह की बात कही जाने लगी है। इसी तरह वहाँ अब प्रबंधन विज्ञान में कहा जाने लगा है – Love men, manage means, जबकि पहले वहाँ कहा जाता था – Love means, manage men.
मनुष्य पर जो अनेक ऋण होते हैं उनमें समाज और निसर्ग का ऋण भी शामिल है। समाज से उऋण होने के लिए समाजसेवा की दृष्टि से दान देने में बचत का सदुपयोग किया जा सकता है। मानव को जब निसर्ग के ऋण की अनुभूति होती है, तब उसका स्वभाव नैसर्गिक संसाधनों का अनाप-शनाप शोषण करनेवाला न होकर आवश्यकतानुसार निसर्ग का दोहन करनेवाला हो जाता है। वह निसर्ग को पूजनेवाला बनता है, निसर्ग को जीतनेवाला नहीं। वह निसर्गमित्र बनता है, निसर्गशत्रु नहीं। यही भारतीय निसर्गदृष्टि है और पर्यावरण से संबंधित
समस्त समस्याओं का उत्तर इसी में है।
हमारे यहाँ अर्थार्जन के अवसर सब को उपलब्ध हो ऐसा विचार है। इसलिए कुटीरोद्योग, स्व-रोजगार, स्व-रोजगार समूह, सहकारिता आधारित उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, बहुराष्ट्रीय उद्योग इत्यादि सब को भारत मैं फलने-फूलने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। हमारे यहाँ ‘योग्यतम की उत्तरजीविता’ (Survival of the fittest) वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, जो पश्चिमी अर्थ तंत्र में साधारणतः होती है। इसलिए प्रत्येक छोटे स्तर के उद्योग की रक्षा हो और उसे फलने-फूलने का अवसर मिले, इस दृष्टि से उससे बड़े स्तर के उद्योगों पर कुछ बंधन और कुछ ‘क्या करें-क्या नहीं’ (Dos Don’ts) होने चाहिए। इसके कारण ‘निर्बलतम की उत्तरजीविका’ (Survival of the weakest) सुनिश्चित होती है, जो हमारी संस्कृति की विशेषता है।
इसके साथ ही कुछ छोटे स्तर के उद्योगों का बड़े स्तर के उद्योगों के लिए अनुपूरक होना सब के फलने-फूलने में सहायक होता है। भारत में विकेंद्रित उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस बात की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है कि यद्यपि अपने यहाँ mass production के स्थान पर production by masses को अधिक महत्त्व दिया जाता है, किन्तु फिर भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ उद्योगों द्वारा mass production किया जाना भी आवश्यक है। ऐसे में किसी भी अतिरेक की ओर न जाते हुए उपरोक्त दोनों में उचित संतुलन बनाये रखने की आवश्यकता है। (कहा ही गया है कि ‘Perfection is not an extreme, it lies in maintaining balance’.)
कोई भी तकनीक अपने साथ दोष भी लाती है। वे दोष न आएँ इस बात की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। इसी तरह बड़े उद्योगों के कारण शहरीकरण बढ़ता है। अपना गाँव छोड़कर शहर आए हुए व्यक्तिपर किसी का नियंत्रण न होने के कारण उसकी अपराधी वृत्ति बढ़ती है। इसलिए अनावश्यक रूप से शहरों की ओर आने की प्रवृत्ति को कम करना होगा। इस दृष्टि से PURA (Providing Urban Facilities in Rural Areas) जैसी योजनाएँ उपयोगी हो सकती हैं।
उत्पादन के अन्यान्य तरीके अपनाकर भरपूर उत्पादन करना चाहिए तथा उत्पादन की उत्कृष्टता के लिए R & D (Research and Development) को पर्याप्त महत्त्व देना चाहिए। उत्पादन के खर्चेपर आधारित लाभकारी मूल्य तो रखना चाहिए, लेकिन सब का सुख हमारा लक्ष्य होने के कारण, वह मूल्य ग्राहक का आर्थिक शोषण करते हुए अत्यधिक लाभ देनेवाला (महंगा) न हो, इस बात
का ध्यान भी रखना पड़ेगा। (इस बात को ‘लाभ में ग्राहक का हिस्सा’ इस रूप में भी लिया जा सकता है और इसीलिए हमारा अर्थशास्त्र ‘सस्ताई’ का है।) साथ ही लाभ का न्यायपूर्ण वितरण पूंजी लगानेवाले, श्रमिक, विभिन्न सेवाएँ देनेवाले और उपयोग में लाए गए प्राकृतिक संसाधनों में किया जाना चाहिए। [हमारी निसर्ग दृष्टि ऐसी है कि उसमें ‘प्रकृति का शोषण’ न करते हुए उसका दोहन किया जाता है। इसके अलावा हमारी दृष्टि केवल प्राप्ति के उपाय जानने तक सीमित नहीं है, ‘giving back’ के मार्गों के बारे में भी उसमें सोचा जाता है। विविध उत्पादन करते समय हम प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकतानुसार दोहन करते हैं, लेकिन ऐसा करते समय भी हम उन्हें नष्ट करते हैं या कम तो करते ही हैं। प्राकृतिक संसाधनों में ‘लाभ का न्यायपूर्ण वितरण’ याने ‘giving back’ के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों की उत्पत्ति / बढ़ोत्तरी हेतु लाभ का कुछ हिस्सा लगाया जाना ।]