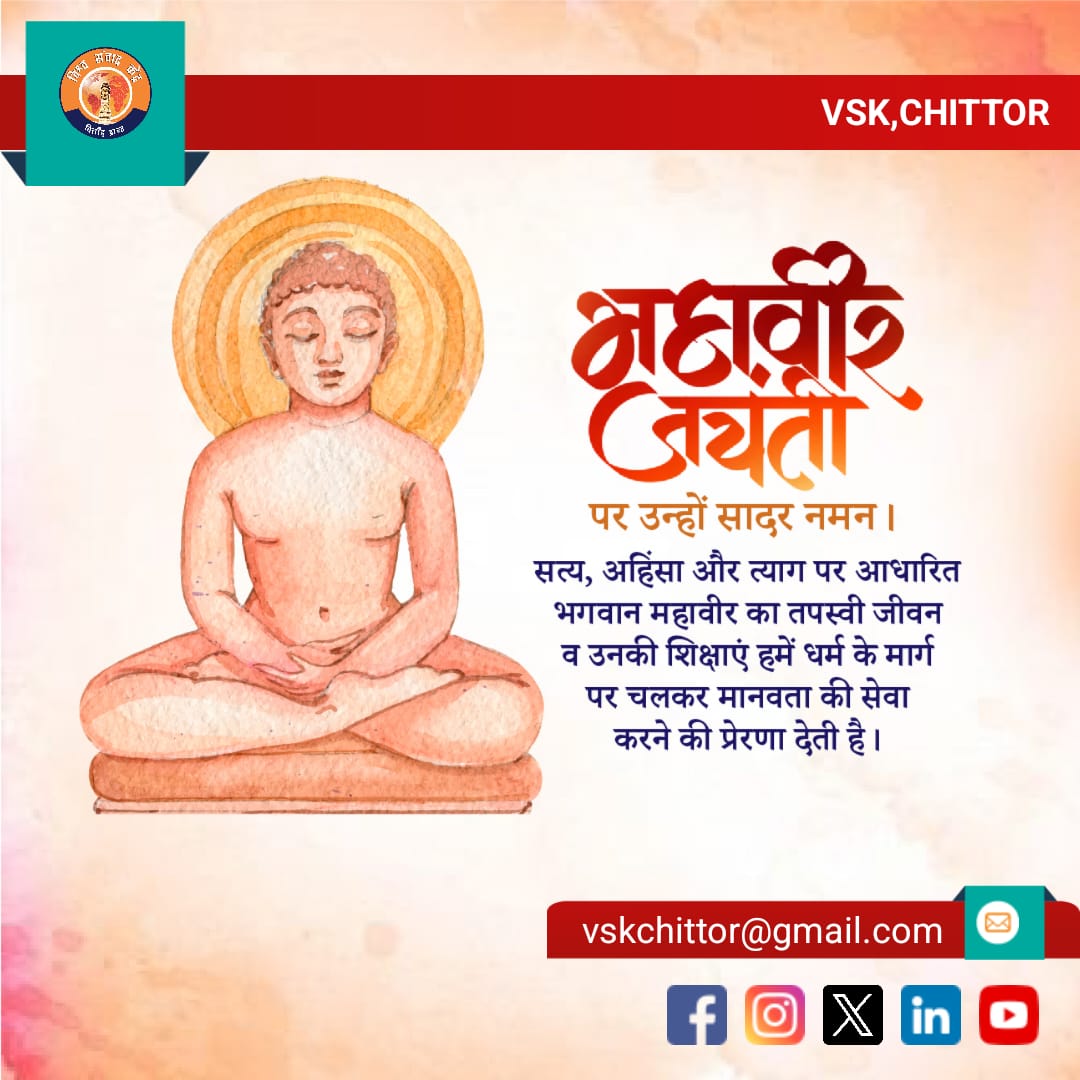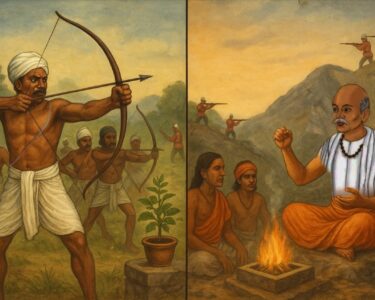भगवान महावीर स्वामी – जैन मत और उसका भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा, सांस्कृतिक उत्थान में योगदान
सिंधु घाटी सभ्यता – योग और भगवान शिव
भारतीय प्राचीन सभ्यता ‘सिन्धु घाटी’ से भी तीर्थंकर ऋषभदेव (भगवान आदिनाथ) का संबंध को मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो प्रतीक प्राप्त हुए हैं, उनमें तीर्थंकर ऋषभदेव के संदर्भ प्रामाणिक रूप में मिले हैं। रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक ‘संस्कृति के चार अध्याय’ में इसी बात की पुष्टि करते हुए लिखते हैं, “मोहनजोदड़ो की खुदाई में योग के प्रमाण मिले हैं और आदि तीर्थकर ऋषभदेव के साथ भी योग तथा वैराग्य की परंपरा जुड़ी हुई है।
दरअसल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर का संबंध भगवान ऋषभदेव से माना जाता है। यह चित्र इस बात का द्योतक है कि आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व योग साधना भारत में प्रचलित थी और इसके प्रवर्तकों में से एक आदि तीर्थकर ऋषभदेव भी शामिल थे।
सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मुहर
अनेक इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि भगवान शिव ही भगवान ऋषभदेव (भगवान आदिनाथ) है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त उपरोक्त मुहर को पशुपति मुहर भी कहा जाता है। दोनों में अनेक समानताएं है जोकि इस बात को पुष्ट करती है। जैसे भगवान शिव का संबंध नंदी यानि बैल से है वैसे ही भगवान ऋषभदेव का चिह्न भी नंदी है। दोनों का चरित्र एवं भेषभूषा भी समान है और दोनों को ही आदि यानि प्रथम माना गया है। योग और वैराग्य का संबंध भी भगवान शिव से जुड़ा है।
इसी तीर्थंकर परंपरा में आगे चलकर भगवान महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था।
ऋग्वेद में तीर्थकर ऋषभदेव
तीर्थकर ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत की घोषणा की थी कि “मनुष्य अपनी शक्ति का विकास कर आत्मा से परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा विद्यमान है जो आत्मसाधना से अपने देवत्त्व को प्रकट कर लेता है वही परमात्मा बन जाता है।“उनकी इस मान्यता की पुष्टि ऋग्वेद की ऋचा से होती है, “जिसके चार शृग – अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनंतसुख और अनंतवीर्य है। तीन पाद हैं – सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यकचरित्र। दो शीर्ष – केवलज्ञान और मुक्ति है तथा जो मन, वचन और कार्य इन तीनों योगों से बद्ध है उस ऋषभ ने घोषणा की कि महादेव (परमात्मा) मानव के भीतर ही आवास करता है।“
जैन तीर्थंकर
भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन, वर्तमान पटना शहर के नजदीक वैशाली (बिहार) में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिसाला के यहाँ हुआ था। उनके माता-पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। उनसे पहले 23 तीर्थकर और हुए उनके नाम इस प्रकार हैं : श्री ऋषभदेव स्वामी, श्री अजीतनाथ स्वामी, श्री संभवननाथ स्वामी, श्री अभिनंदन स्वामी, श्री सुमतिनाथ स्वामी, श्री पद्मप्रभ स्वामी, श्री सुप्रश्वंरथ स्वामी, श्री चंद्रप्रभ स्वामी, श्री सुविदेव स्वामी, श्री शीतलनाथ स्वामी, श्री श्रेयांसनाथ स्वामी, श्री वासुपूज्य स्वामी, श्री विमलनाथ स्वामी, श्री अनंतनाथ स्वामी, श्री दरमनाथ स्वामी, श्री शत्रुनाथ स्वामी, श्री कुंतुनाथ स्वामी, श्री अराध्य स्वामी, श्री मल्लीनाथ स्वामी, श्री मुनिसुव्रत स्वामी, श्री नमिनाथ स्वामी, श्री नेमनाथ स्वामी, श्री पार्श्वनाथ स्वामी और श्री वर्धमान महावीर स्वामी।
जैन मत के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी से पहले और उनके बाद भी जैन मत का भारतीय ज्ञान परंपरा के क्रमिक एवं सतत विकास सहित भारतीय संस्कृति के उद्भव में अभूतपूर्व योगदान रहा है।
भारत के प्राचीन नगरों से संबंध
जैन मत के अधिकांश तीर्थकरों का जन्म भारत के प्राचीन शहरों में हुआ। ये प्राचीन शहर भारतीय ज्ञान परंपरा सहित सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। उदाहरण के लिए भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ, भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ, भगवान शांतिनाथ जोकि 16वें तीर्थकर थे, उनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ। 19वें तीर्थकर भगवान मल्लिनाथ का जन्म मिथिला में हुआ।
श्रमण परंपरा
भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति पावन गंगा के समान है, जिसमें दो महान नदियाँ आकर मिली हैं – श्रमण और वैदिक। इन दोनों के संगम से विशाल भारतीय संस्कृति की गंगा बनी है। प्राचीन साहित्य में जैन धर्म के लिए ‘श्रमण’ शब्द का प्रयोग मिलता है। (जो श्रम करता है, कष्ट सहता है, तप करता है वह ‘श्रमण’ कहलाता है)।
श्रीमदभागवत में श्रमणों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जो वातरशन श्रमण मुनि है, वे शांत, निर्मल, सम्पूर्ण परिग्रह से सन्यस्त ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। भूषण टीका में श्रमण शब्द की व्याख्या इस रूप में की गई है – ‘श्रमणा दिगम्बराः श्रमणा वातरशनाः’।
श्रमण ‘दिगम्बर’ मुनि होते हैं। उन मुनियों को ही भागवतकार ने वातरशना, आत्मविद्या में विशारद बताया है। भारत में श्रमणों का अस्तित्व प्राचीन काल से है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में श्रमणों का उल्लेख मिलता है। श्री वाल्मीकि रामायण में भी अनेक स्थानों पर श्रमणों का उल्लेख बड़े सम्मान के साथ किया गया है। भगवान राम ने जिन माता शबरी के आतिथ्य को ग्रहण किया था, वह श्रमणी थी। माता सीता के पिता, राजा जनक जिस तापसों को भोजन कराते थे, श्रमणों को भी वैसे ही कराते थे। श्रमण आत्मविद्या में पारंगत थे। वैदिक ऋषि उनसे आत्मविद्या सीखते थे। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार “श्रमण परंपरा के कारण ब्राह्मण धर्म में वानप्रस्थ और संन्यास को प्रश्रय मिला।“ वस्तुतः प्राचीन काल में जैनों को ही श्रमण कहा जाता था।
वैदिक ग्रंथों में जैनधर्मानुयायियों को अनेक स्थलों पर ‘व्रात्य’ भी कहा गया है। व्रतों का आचरण करने के कारण वे व्रात्य कहे जाते थे। संहिता काल में व्रात्यों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। व्रात्यों की प्रशंसा ऋग्वेद काल से लेकर अथर्ववेद काल तक प्राप्त होती है। अथर्ववेद में तो स्वतंत्र ‘व्रात्य सूक्त’ की रचना भी मिलती है।
जैन मत में श्रमण और व्रात्य शब्दों के समान आर्हत शब्द का प्रयोग भी प्राचीन काल से होता आया है। श्रीमदभागवत में तो आर्हत शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर हुआ है। एक स्थान पर भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में लिखा है, “तपाग्नि से कर्मों को नष्टकर वे सर्वज्ञ ‘अर्हत’ हुए और उन्होंने आर्हत मत का प्रचार किया।“ मत्स्यपुराण में बताया है कि अहिंसा ही परम धर्म है, जिसे अर्हन्तों ने निरुपित किया है। वस्तुतः प्राचीन ज्ञान परंपरा में ‘आर्हतमत’ और ‘अर्हन्तों’ का उल्लेख मिलता है। ‘श्रमण’, ‘व्रात्य’ और ‘आर्हत’ इन तीनों शब्दों का प्रयोग जैन मत के लिए ही किया गया है।
श्रमण परंपरा के प्रतिष्ठापकों में महावीर स्वामी का एक अन्यतम स्थान है।
महिला तीर्थंकर!
ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर मल्लिनाथ एक महिला थे। हालांकि दिगम्बर ऐसा नहीं मानतें हैं, जबकि श्वेताम्बर परंपरा में यह माना गया है। अगर यह तथ्य सटीक है तो यह इस ओर संकेत करता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा है। हजारों साल पहले भारत में एक महिला को तीर्थकर का दर्जा देना इसी बात का प्रमाण है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अनेक ऐसी विदुषी महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रमाण प्रस्तुत किए है।
महाभारत कालखंड
तीर्थंकर नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) के विषय में एक ऐतिहासिक तथ्य है। वह भगवान श्रीकृष्ण के चचेरे भाई हैं। भगवान श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव और उनके बड़े भाई समुद्रविजय के पुत्र नेमिनाथ थे। उनकी माता का नाम शिवा देवी था। तीर्थंकर नेमिनाथ का उल्लेख सामवेद में भी प्राप्त होता है।
अहिंसा और जैन मत
जर्मन अध्येता डॉ. हरमन याकोबी ने तीर्थंकर पार्शवनाथ को अहिंसा के सफल प्रणेता के तौर पर माना है। धर्मानंद कौशांबी ने भगवान पार्शवनाथ पर ‘पार्शवनाथा चा चारयाम’ पुस्तक लिखी है। उन्होंने भी तीर्थंकर पार्शवनाथ को अहिंसा के प्रणेता के रूप में स्वीकार किया है। वह यह भी सिद्ध करते है कि भगवान बुद्ध ने भगवान पार्शवनाथ कि परंपरा से ही अहिंसा का पाठ ग्रहण किया था। उसी अहिंसा को पंचशील के नाम से विख्यात कर दिया अथवा उसका नाम अष्टांगयोग दिया। इस तथ्य के अनुसार अहिंसा का मार्ग भारत में महात्मा बुद्ध से पहले भी प्रचलित था। भगवान बुद्ध को अहिंसा की शिक्षा भगवान पार्श्वनाथ से ही प्राप्त हुई है। भगवान पार्श्वनाथ ने भारत में अहिंसा का बहुत ही विस्तृत प्रचार-प्रसार किया था।
रामायण के रचियता
भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग चार शताब्दियों के बाद राजा विक्रमादित्य के शासन में जैन विद्वान विमलसूरी ने प्राकृत भाषा में ‘पउमचरिउ’ (पदम्चरित –जैन रामायण) की रचना की। इससे प्रतीत होता है कि उस समय रामायण की कथा जनता में अत्यंत लोकप्रिय थी। विमलसूरी ने रामायण का जैन-संस्करण लिखा था।
संस्कृत साहित्य और जैनाचार्य
भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन में जैन मत का विशेष योगदान रहा है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण पुराणों सहित अन्य भारतीय ग्रंथों में मौजूद हैं। योगवशिष्ठ, श्रीमदभागवत, विष्णुपुराण, पदम्पुराण, मत्स्यपुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में जैन मत का उल्लेख मिलता है।
भारतीय संस्कृत साहित्य का अधिकांश भाग जैन-ग्रन्थ भण्डारों में सुरक्षित है। जैसलमेर, नागौर एवं बीकानेर के ग्रन्थागार इस तथ्य के साक्षी हैं। इन ग्रन्थागारों के द्वारा संस्कृत साहित्य के इतिहास की कड़ियाँ प्रकाश में आ सकी हैं। संस्कृत के रचनाकारों के साथ-साथ हमें महामना जैन मुनियों का भी ऋणी होना चाहिए, जिन्होंने अपने संस्कृतानुराग के कारण कई दुर्लभ एवं विस्मत संस्कृत ग्रन्थों पर ध्यान केन्द्रित कर उन्हें काल के भयंकर थपेड़ों से और इतिहास की खूखार तलवार से बचाये रखा। डॉ. सत्यव्रत ने ठीक ही कहा है, “यह सुखद आश्चर्य है कि जैन साधकों ने अपने दीक्षित जीवन तथा निश्चित दृष्टिकोण की परिधि में बद्ध होते हुए भी साहित्य के व्यापक क्षेत्र में झाँकने का साहस किया, जिसके फलस्वरूप वे साहित्य की विभिन्न विधाओं एवं उसकी विभिन्न शैलियों की रचनाओं से भारती के कोश को समृद्ध बनाने में सफल हुए हैं।”
महावीर स्वामी के बाद जैन परंपरा मेंन आचार्य पादलिप्त का उल्लेख सामने आता है। उनका कालखंड ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य के आसपास माना गया है। उन्होंने प्राकृत भाषा में एक बहुत ही सुन्दर रचना ‘तरंगावली’ के नाम से लिखी है। यह पुस्तक मूलतः जैन महाराष्ट्रीय प्राकृत में निर्माण की गई है। गद्य और पद्य दोनों का ही विलक्षण समन्वय इसमें किया गया है। आचार्य वीरभद्र के शिष्य नेमनाथ ने इसे प्राकृत में ही 100 गाथा परिमाण का संक्षिप्त संस्करण तैयार किया है। इसके अतिरिक्त जैन नित्यकर्म, जैन दीक्षा, प्रतिष्ठा-पद्धति तथा शिल्प-निर्माण-कलिका नामक ग्रंथों को आचार्य देव ने संस्कृत भाषा में ही लिखा है। सम्राट विक्रमादित्य वैदिक परंपरा को मानते थे लेकिन उनके शासन में अन्य मतों को भी पूरा सम्मान मिलता था। उनके नवरत्नों में एक जैन संत सिद्धसेन दिवाकर भी शामिल थे।
11-12वीं शताब्दी में होने वाले आचार्य हेमचन्द्र संस्कृत के उद्भट विद्वान् थे। संस्कृत वाङमय के क्षेत्र में आचार्य हेमचन्द्र का विस्मयकारी योगदान है। प्रमाणमीमांसा उनकी जैनन्याय की अनूठी रचना है। त्रिशष्टिशलाका पुरुषचरित प्रसिद्ध महाकाव्य है। सिद्धहेमशब्दानुशासन लोकप्रिय व्याकरणग्रंथ है। जैनाचार्य ब्रह्म जिनदास ने हिन्दी के साथ संस्कृत भाषा में भी काव्य रचना की, जिनमें पद्मपुराण, जम्बूस्वामीचरित्र, हरिवंशपुराण मुख्य हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के सम्वर्धन में जैन मुनियों, आचार्यों एवं विद्वानों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
कन्नड भाषा से संबंध
कन्नड़ भाषा के जन्मदाता, उसके साहित्य को समृद्ध करने बाले ओर कन्नड़ की महानतम देन, देने वाले जैन कवि ही थे। इस समस्त धार्मिक प्रचार, प्रभाव एवं सम्रद्धि का श्रेय महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के प्रमुख आचार्य भद्गबाहु स्वामी को है, जिन्होंने अनेक उपसर्ग सहन कर आहँती संस्कृति का प्रचार किया।
काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण
1206 में गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुलतान कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। इसके बाद 1260 तक तुर्कों का काशी पर कब्जा बना रहा। हालाँकि, इसी समयाविधि में हिन्दुओं ने स्थानीय स्तर पर अपना दबदबा फिर से बना लिया था। इसका एक उदाहरण इल्तुतमिश के शासन में मिलता है। दरअसल, गुजरात के एक जैन दानकर्ता वास्तुपाल द्वारा विश्वनाथ मंदिर की पूजा के लिए धनराशि भेजने का उल्लेख मिलता है। यह पैसे उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के पुनः स्थापना के लिए भेजे थे।
महावीर स्वामी – तपस्वी जीवन
भगवान महावीर ने सत्य की खोज के लिए राजसी वैभव को त्यागकर बारह वर्ष तपस्वी के रूप में बिताए। उन्होंने अपना अधिकांश समय ध्यान करने और लोगों के बीच अहिंसा का प्रचार करने में बिताया और सभी प्राणियों के प्रति श्रद्धा भाव रखा। महावीर स्वामी ने एक अत्यंत तपस्वी जीवन चुना, तपस्या करते हुए उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया।
महावीर ने अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आसक्तियों पर विजय पाने के लिए अगले साढ़े बारह साल गहन मौन और ध्यान में बिताए। उन्होंने सावधानीपूर्वक जानवरों, पक्षियों और पौधों सहित अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने से परहेज किया। वह लंबे समय तक बिना भोजन के भी रहे। वह सभी असहनीय कठिनाइयों के बावजूद शांत और शांतिपूर्ण थे, इसलिए उन्हें महावीर नाम दिया गया, जिसका अर्थ है बहुत बहादुर और साहसी। इस अवधि के दौरान, उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई और अंत में उन्हें पूर्णज्ञान, शक्ति और आनंद का एहसास हुआ। इस अनुभूति को केवलज्ञान या पूर्णज्ञान के रूप में जाना जाता है।
महावीर ने अगले तीस साल पूरे भारत में नंगे पैर यात्रा करते हुए लोगों को उस शाश्वत सत्य का प्रचार करते हुए बिताये जिसे उन्होंने महसूस किया था। उनकी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति जन्म, जीवन, दर्द, दुःख और मृत्यु के चक्र से पूर्ण स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है और स्वयं की स्थायी आनंदमय स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसे मुक्ति, निर्वाण, पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष के रूप में भी जाना जाता है।
जैन मत के श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार वर्द्धमान की मां को 14 सपने आए थे। ज्योतिषियों ने जब इन सपनों की व्याख्या की तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो सम्राट बनेगा या तीर्थंकर। ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां सच निकली और वह बाद में जैन मत के 24वें तीर्थंकर बन गए।
भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं
अहिंसा – किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुँचाना; सत्य – केवल हानिरहित सत्य बोलना; अस्तेय – जो कुछ भी ठीक से नहीं दिया गया है उसे न लें; ब्रह्मचर्य – (शुद्धता): कामुक आनंद न लेना; और अपरिग्रह : लोगों, स्थान और भौतिक चीजों से पूरी तरह से अलग होना।
कर्म प्रधान व्यक्तित्व
आज के परिवेश में हम जिस प्रकार की समस्याओं और जटिल परिस्थितियों में घिरे हैं, उन सभी का समाधान महावीर के सिद्धांतों और दर्शन में समाहित है। महावीर स्वामी कहा करते थे कि जिस जन्म में कोई भी जीव जैसा कर्म करेगा, भविष्य में उसे वैसा ही फल मिलेगा। वह कर्मानुसार ही देव, मनुष्य व पशु-पक्षी की योनि में भ्रमण करेगा। कर्म स्वयं प्रेरित होकर आत्मा को नहीं लगते बल्कि आत्मा कर्मों को आकृष्ट करती है। वह कहते हैं कि रुग्णजनों की सेवा-सुश्रुषा करने का कार्य प्रभु की परिचर्या से भी बढ़कर है। अपने जीवनकाल में उन्होंने ऐसे अनेक उपदेश दिए, जिन्हें अपने जीवन तथा आचरण में अपनाकर कर हम अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं।
जीओ व जीने दो
महावीर स्वामी का मानना है कि जो मनुष्य स्वयं प्राणियों की हिंसा करता है या दूसरों से हिंसा करवाता है अथवा हिंसा करने वालों का समर्थन करता है, वह जगत में अपने लिए बैर बढ़ाता है। उन्होंने अहिंसा की तुलना संसार के सबसे महान व्रत से की है और कहा है कि संसार के सभी प्राणी बराबर हैं, अतः हिंसा को त्यागिए और ‘जीओ व जीने दो’ का सिद्धांत अपनाइए। वह कहते हैं कि संसार में प्रत्येक जीव अवध्य है, अतः आवश्यक बताकर की जाने वाली हिंसा भी हिंसा ही है और वह जीवन की कमजोरी है।
महावीर स्वामी के अनुसार किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही ज्ञानी होने का एकमात्र सार है और यही अहिंसा का विज्ञान है। जिस प्रकार अणु से छोटी कोई वस्तु नहीं और आकाश से बड़ा कोई पदार्थ नहीं, उसी प्रकार अहिंसा के समान संसार में कोई महान व्रत नहीं। महावीर स्वामी के शब्दों में कहें तो ज्ञानी होने का यही एक सार है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे और यही अहिंसा परम धर्म है।
भगवान् महावीर का मानना है कि प्रत्येक जीवित व्यक्ति के प्रति दया भाव रखो क्योंकि घृणा करने से स्वयं का विनाश होता है।
जाति – जन्म से नहीं कर्म से
धर्म को लेकर महावीर स्वामी का मत है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है और अहिंसा, तप व संयम उसके प्रमुख लक्षण हैं। जिन व्यक्तियों का मन सदैव धर्म में रहता है, उन्हें देव भी नमस्कार करते हैं। अपने उपदेशों में वह कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद यदि कर्म श्रेष्ठ हैं तो वही व्यक्ति ब्राह्मण है किन्तु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि वह हिंसाजन्य कार्य करता है तो वह ब्राह्मण नहीं है जबकि नीच कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर सुआचरण, सुविचार एवं सुकृत्य करता है तो वह बाह्मण है।
पर्यावरण संरक्षण
महावीर स्वामी का मत है कि मानव और पशुओं के समान पेड़-पौधों, अग्नि, वायु में भी आत्मा वास करती है और पेड़-पौधों में भी मनुष्य के समान सुख-दुख अनुभव करने की शक्ति होती है।