स्वतन्त्रता दिवस के संदर्भ में RSS के पू सरसंघ चालक द्वारा दिये गए वक्तव्य “स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक” पर आधारित लेख माला। लेख सदानन्द सप्रे जी की पुस्तक से लिया गया है। इस श्रंखला का ये 7वां लेख प्रस्तुत है।
स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक
स्वतन्त्रता नियमित चलने वाली प्रक्रिया है।
आज का विषय- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी– 7
भारत की ज्ञान परंपरा में आत्मा से संबंधित बातों के अध्ययन को ‘विद्या’ और जिसका आत्मा से संबंध नहीं है ऐसी जड़ सृष्टि के अध्ययन को ‘अविद्या’ कहते हैं (जिसके अंतर्गत अन्यान्य बातों के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी आते हैं।) प्रचलित धारणा के विपरीत, भारत में विद्या और अविद्या इन दोनों को ही महत्त्व दिया गया है, केवल विद्या को नहीं; क्योंकि दोनों परस्परपूरक हैं और इसलिए मानव जीवन में दोनों ही आवश्यक हैं। ईशोपनिषद में तो कहा गया है कि-
“विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदोभयं सह
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।”
(जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर के विद्या से अमृतत्व याने देवत्व प्राप्त कर लेता है।) – इसलिए भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में (तक्षशिला, नालन्दा, पुष्पगिरि, नागार्जुनकोंडा, वल्लभी, सोमपुरा, कंठल्लूर, नादिया इत्यादि – जो सही अर्थ में विश्वविद्यालय थे, जहाँ सारे विश्व के ज्ञानपिपासु अध्ययन करने के
लिए आते थे) विद्या और अविद्या इन दोनों का अध्ययन-अध्यापन होता था।
हजारों वर्षों तक तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में (जो अविद्या के अंतर्गत आते हैं) प्राप्त उन्नत अवस्था के कारण भारत अत्यंत समृद्ध था, जिस कारण इस ‘सोने की चिड़िया’ को लूटने के लिए बार-बार विश्वभर के लुटेरे आते रहे। सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक धर्मपाल जी द्वारा लिखित अत्यंत शोधपूर्ण ग्रंथ ‘१८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान और तंत्रज्ञान’ में सप्रमाण यह बताया गया है कि १८ वीं सदी के विश्वव्यापार में भारत सर्वोपरी था (जबकि उस
समय तक शक, हूण, यवन, कुषाण इत्यादी दुनियाभर के लुटेरे इस सोने की चिड़िया को लूट चुके थे और अरब, तुर्क, मंगोल, मुगल इत्यादि लुटेरे शासन के •माध्यम से भी इसे लूट रहे थे) ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत द्वारा उन्नत अवस्था प्राप्त करने का प्रमुख कारण है- भारत की जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की तथा स्वयं प्रयोग और चिंतन द्वारा उसका समाधान और उत्तर खोजने की परंपरा, जिसे समाज द्वारा सदैव प्रोत्साहन दिया गया। (वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे R & D – Research and Development मानसिकता कहा जा सकता है।) अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इस परंपरा और मानसिकता को बढ़ाना होगा। ‘आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः’ के अनुसार जहाँ से भी मिले, अच्छा ज्ञान तो प्राप्त करना होगा; लेकिन स्वचिंतनके आधारपर उसे स्वानुकूल बनाकर अपनाना होगा। इस दृष्टि से ‘सीखना और नकल करना’ तथा ‘Adapt और Adopt’ के बीच के अंतर को हमें ध्यान में रखना होगा।
ज्ञान को स्वानुकूल बनाते समय हमें भारतीय चिंतन और वर्तमान भारत की आवश्यकताओं के बारे में विचार करना होगा। ‘सब का सुख’ और ‘संपूर्ण चराचर सृष्टि का मंगल’ यह हमारा लक्ष्य होने के कारण हमें उसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। आधुनिक तकनीक के आधारपर देश आगे बढ़ता है और उसका विकास होता है। परन्तु हमारा मार्ग पश्चिम के मार्ग से भिन्न होना चाहिए इस बात को जानने की आवश्यकता है। भारत का परिवेष और आवश्यकताओं को देखते हुए हमारी प्रौद्योगिकी कम पूंजीवाली, कम ऊर्जाभक्षी, टिकाऊ (sustainable), रोजगारोन्मुख, विकेंद्रित, पर्यावरण सुसंगत तथा मानवीय चेहरा लिए हुए होनी चाहिए। आज के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीवेत्ताओं के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है।
भारत में लंबे समय से बड़े पैमाने पर ग्रामीण और स्वदेशी तकनीक का उपयोग होता रहा है। इन में आधुनिक बातें जोड़ते हुए नवाचार (innovation) को प्रोत्साहन देने से ग्रामीण और स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
पश्चिमी विकासपथ में विकास और पर्यावरण में संघर्ष है, जबकि भारतीय विकासपथ में विकास और पर्यावरण में सामंजस्य है। इसका कारण है, सृष्टि की ओर देखने का अलग-अलग दृष्टिकोण। पश्चिमी चिंतन में माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण मानव के उपभोग के लिए किया गया है; इसलिए मानव की
इच्छाओं, तृष्णाओं की पूर्ति के लिए सृष्टि का अमर्यादित शोषण किया जा सकता है। भारतीय चिंतन में व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्ठि में एकात्मता ऐसा विचार है, इसलिए मानव का सृष्टि की ओर देखने का दृष्टिकोण आवश्यकतानुसार दोहन करनेवाला है। इसे तो सब स्वीकार करते हैं कि सृष्टि द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है; उसकी इच्छाओं, तृष्णाओं की नहीं। (The nature has enough to fulfil our needs, not our greeds.)
भारतीय चिंतन के अनुसार सब कुछ धर्मनियंत्रित (धर्मसुसंगत) होना चाहिए। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी धर्मनियंत्रित होने चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ज्ञानपर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और चूँकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान की शाखाएँ हैं इसलिए उनपर भी किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। परन्तु धर्म याने समाज की धारणा । इसलिए जिन बातों से समाज और सृष्टि की धारणा में बाधा उत्पन्न होती है (याने समाज और सृष्टि का अहित होता है) वे बातें नहीं होनी चाहिए, भले ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी वे बातें करने में सक्षम हों।
आज के जगत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध (नियंत्रण) के अनेक उदाहरणों में से कुछ उदाहरण देखे जाएँ –
१) गर्भस्थ भ्रूण के लिंग परीक्षण की मनाही । यद्यपि विज्ञान यह कर सकता है, परंतु फिर भी इस बात की मनाही है; क्योंकि उसके कारण कन्या भ्रूण का गर्भपात किया जा सकता है, जो अनैतिक होने के अलावा समाज के लिए अहितकारी भी है।
२) आतंकवादी संगठन और देशों के पास परमाणु हथियार न हों इस प्रकार के नियम हैं, क्योंकि उन के पास ऐसे हथियार होना यह मानवता के लिए बड़ा खतरा है।
३) कारखानों में पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित अनेक प्रतिबंध होते हैं, क्योंकि उन के न होने से सृष्टि को और मानव के स्वास्थ्य को खतरा है। इसलिए मानवहित और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी
पर भी धर्म का नियंत्रण आवश्यक है। समय की आवश्यकताओं के अनुसार धर्म के नियंत्रण से संबंधित बातें निर्धारित करने के अलावा समय-समय पर उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए।
पश्चिम के विकासपथ के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जिनमें से पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने का प्रयास तो दुनियाभर के चिंतक कर रहे हैं Earth Summit, Global Environment Meet इत्यादि के माध्यम से। नोबल पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद् श्री. अल गोर (अमरीका के पूर्व उपराष्ट्रपति) ने स्वीकार किया है कि, ‘We have been on the wrong track for last three hundred years. ( पश्चिमी विकासपथ ३०० वर्ष पुराना है।) It’s time to rethink and turn to East (याने भारत) for guidance.’ अतः भारत के सामने यह चुनौती है कि पश्चिमी विकासपथ की नकल न करते हुए भारतीय चिंतन के अनुसार धर्म नियंत्रित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर अपना विकास करें, ऐसा विकास जो पर्यावरण सुसंगत होने के साथ ही सब प्रकार की समस्याओं से मुक्त तथा सर्वजनहिताय-सर्वजनसुखाय हो। ऐसा विकसित भारत संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है (अल गोर के कहे अनुसार ) ।


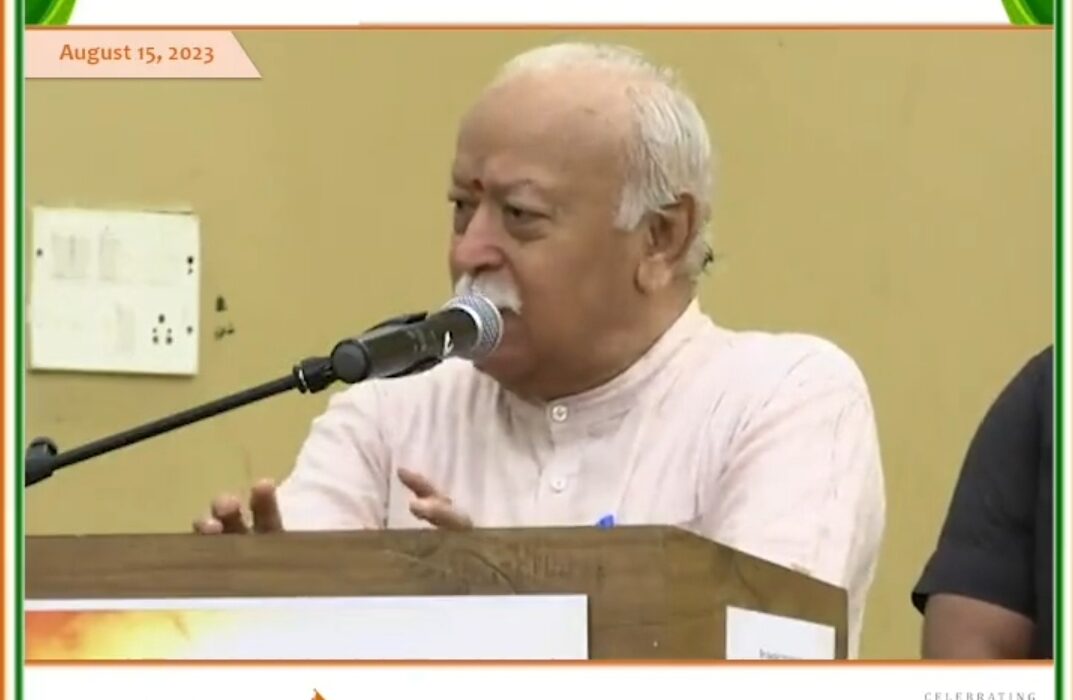


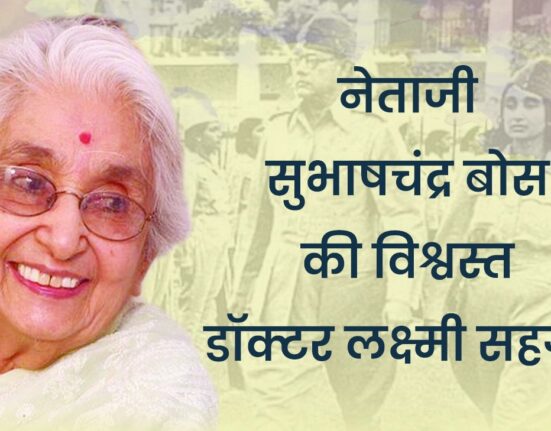



Leave feedback about this