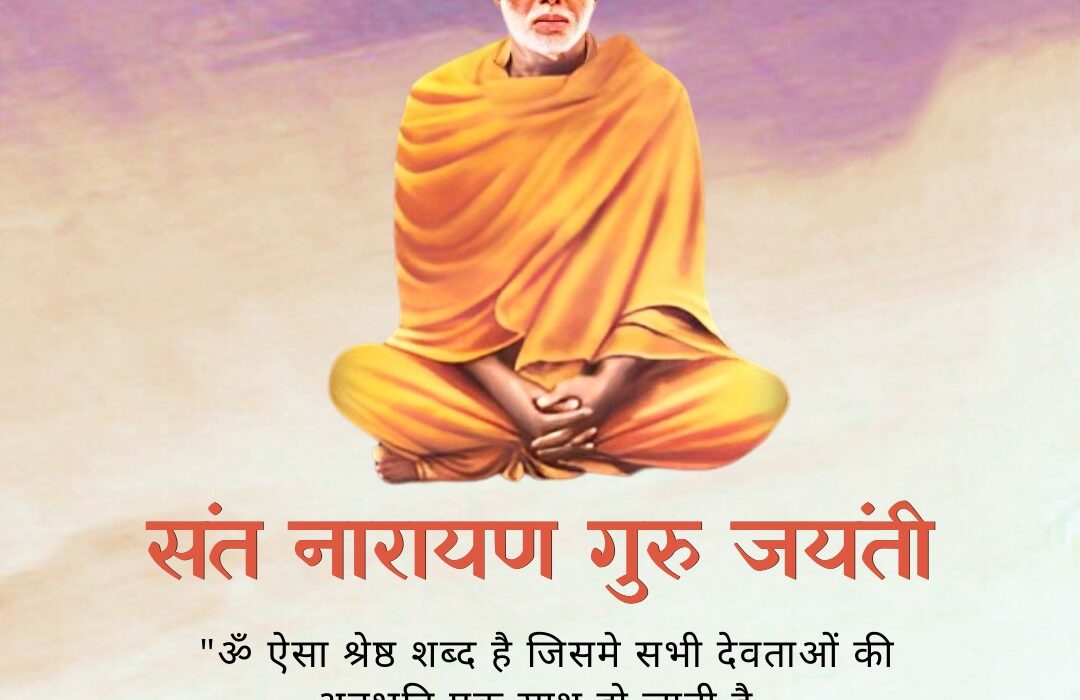श्री नारायण गुरु जयंती “20 अगस्त, 1856”
कार्यकारी सारांश
श्री नारायण गुरु भारत के एक महान संत, विद्वान, दार्शनिक, कवि और देश के दक्षिणी क्षेत्रों में सामाजिक पुनर्जागरण और सौहार्द के अग्रदूत थे। वह अपने वैदिक ज्ञान, काव्य प्रवीणता, और सामाजिक दोषों को ठीक करके उसके स्थान पर सही व्यवस्था स्थापित करने के अडिग संकल्प जैसे गुणों के लिए पूजे जाते है। नारायण गुरु ने केरल में सामाजिक सुधार के लिए आध्यात्मिक नींव स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह भारत जातिगत भेदभाव को दूर करने के प्रयासों को गति देने वाले सबसे सफल समाज सुधारकों में से एक थे । उन्होंने आपसी संघर्ष के बिना सामाजिक मुक्ति के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। नारायण गुरु अन्य समाज सुधारकों से एक भिन्न प्रकृति के समाज सुधारक थे, जिन्होंने सदैव समग्रता मूलक समाधान प्रस्तुत किए जिसमें उन्होने लोगों को एक दूसरे का विरोधी या शत्रु के रूप में चिह्नित नहीं किया।
मुख्य बिंदु
नारायण गुरु के कथन
मंदिर
- जिन उद्देश्यों के लिए मंदिर बनाए गए थे, क्या व्यवहार में उन्हें अनुभव किया गया है? ईश्वर की पूजा मात्र मंदिरों में ही नहीं होनी चाहिए बल्कि इन्हें प्रत्येक हृदय मे विराजमान होना चाहिए।
पशु बलि - सभी सजीव प्राणी एक भ्रातृत्व का निर्माण करते हैं। यह जीवन का नियम होना चाहिए । ऐसा होने के कारण हम पशुओं की बलि कैसे दे सकते हैं?
- जैसे कि कहा गया है कि सभी जीव एक स्व-बिरादरी के हैं, इस तथ्य के आलोक में हम किसी जीव का जीवन कैसे ले सकते हैं और दया से रहित होकर उन्हे कैसे खा सकते हैं?
पूजा - भगवान की पूजा कहीं भी की जा सकती है। मूर्तियां हमेशा आवश्यक नहीं हैं। यही वह आदर्श है जो कि अर्थ रखता है ।
- अपने सभी मंदिरों में सत्य और प्रेम के साथ-साथ कर्तव्यनिष्ठा की घोषणा करें। इसे अपनी जीवनशैली में भी एक अभिन्न अंग बना लें।
शराब की बुराई - शराब विष की तरह ही एक बुराई है। इसका निर्माण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसे न तो किसी को प्रस्तुत करना चाहिए और न ही स्वयं पीना चाहिए।
शिक्षा एवं लैंगिक समानता - शिक्षा उस हर किसी के लिए एक साधन है जो इस संसार में प्रगति की इच्छा रखता है । इसलिए इसे सभी को देना होगा। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी शिक्षित होना चाहिए।
- शिक्षा के माध्यम से प्रगति करें और संगठन के माध्यम से सशक्त बनें।
आर्थिक सामाजिक समृद्धि - अगर लोग स्वयं को उद्यम में सम्मिलित नहीं करते हैं तो किसी देश की सम्पदा नहीं बढ़ सकती । हमारे बच्चों को औद्योगिक स्कूलों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
जाति पर - मानव प्रजाति के लिए मात्र एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर
- जाति-न पूछो, न बोलो और न ही सोचो
- कोई व्यक्ति जो कार्य अपने स्वयं के लिए करता है उसका एक लक्ष्य अन्य लोगों की भलाई भी होना चाहिए
मानव जाति के लिए प्रेम पर - दूसरों का प्रेम मेरी प्रसन्नता है, मेरा जो प्रेम है वह दूसरों के लिए प्रसन्नता है। इस प्रकार, वास्तव में, एक कर्म जो एक व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है वह दूसरों की भी प्रसन्नता का कारण होना चाहिए।
- अनुग्रह, प्रेम , दया-ये तीनों एक ही वास्तविकता (जीवन का प्रकाशीय तत्व ) का प्रतिनिधित्व करते है। वह जो प्रेम करता है वही वास्तव में जीवन को जीता है ।
- मनुष्यों के पंथ, पहनावे और भाषा आदि में चाहे जो भी अंतर हो किन्तु वे सभी एक ही तरह की सृष्टि के अंग हैं, इसलिए उनके एक साथ खाने या एक-दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध रखने में कोई बुराई नहीं है ।
- जाति या नस्ल या आस्था की प्रतिद्वंदिता की घृणा की दीवारों को विभाजित करने से मुक्त होकर हम सब यहां भाईचारे में रहते हैं
- हमारी उंगलियों, हाथों और पैरो को हमेशा काम ढूंढना चाहिए। वे बेचैन घोड़ों की तरह हैं। यदि हम उन्हें पर्याप्त कार्य में संलग्न नहीं रखते हैं, तो हम बीमार पड़ जाएंगे ।
जीवनी
श्री नारायण गुरु का जन्म 20 अगस्त, 1856 को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन राज्य त्रावणकोर और वर्तमान भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित गांव चेम्पाझंथी में मदन आसन और उनकी पत्नी कुटियाम्मा के पुत्र के रूप हुआ था। 20 अगस्त, 1856 को ‘व्यालवरम’ नामक एक किसान परिवार में पैदा हुए बच्चे का नाम ‘नानू’ रखा गया जिसका अर्थ है ‘नारायण’।
उनके पिता मदन को “आसन” उपनाम इसलिए मिला क्योंकि वह न केवल एक किसान थे बल्कि एक ‘आसन’ भी थे। संस्कृत भाषा से व्युत्पन्न मलयालम शब्द ‘आसन’ का अर्थ है ‘आचार्य’- एक शिक्षक। वह संस्कृत जानते थे और उन्होंने ज्योतिष और आयुर्वेद का अध्ययन किया था। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वह ग्राम वासियों को कई महत्वपूर्ण प्रकरणों में यथोचित पर सलाह देकर उनकी सहायता किया करते थे। उनकी वेषभूषा अत्यंत साधारण थी। वह कमर के चारों ओर ढकने के लिए कपड़े का टुकड़ा लपेटते थे और शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए कपड़े का टुकड़ा पहनते थे।
जब कभी वह घर से बाहर निकलते तो वह अपने साथ एक ताड़ के पत्ते का छाता लेकर जाते थे । केरल में उन दिनों यही रिवाज प्रचलन में था।
चूंकि मदन आसन संस्कृत में पारंगत थे , इसलिए वह रामायण और महाभारत को अच्छी तरह से जानते थे। वह सप्ताह में एक बार सरल भाषा में उन पर प्रवचन देते थे, अपने घर के बरामदे में बैठते थे। गांव के लोग बड़ी रुचि के साथ इकट्ठा होकर उसकी बातें सुनते थे। नानू भी अपने पिता के प्रवचन बड़ी चाव से सुनते थे । कई बार जब मदन प्रवचन के लिए उपस्थित नहीं तो उस समय स्वयं नानू को प्रवचन देना पड़ता था।
नानू की मां अपने नाम ‘कुट्टी’ यानि ‘दाग दोष रहित निष्कलंक’ को चरितार्थ करती थी। वह बुद्धिमान और दयालुता से भरी एक निष्कपट महिला थी। वह अपने काम में शांतचित्त थी । नानू की प्रारंभिक शिक्षा चेमपाहांथीमुथापिल्लई के आचार्यत्व में गुरुकुल पद्धति से हुई। शिक्षा ग्रहण के समय जब उनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी, उसी समय उनकी माता का देहांत हो गया। 21 साल की आयु में वह संस्कृत के विद्वान रमन पिल्लई आसन से उच्चतर शैक्षिक ज्ञान सीखने के लिए केंद्रीय त्रावणकोर गए थे जिन्होंने उन्हे वेद, उपनिषद और संस्कृत के साहित्य और तार्किक अलंकार शास्त्र सिखाया। 1881 में जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, तब वे अपने गाँव लौट आए और वहाँ एक स्कूल शुरू किया जिसमे वह स्थानीय बच्चों को पढ़ाते थे, जिससे उनका नाम नानू आसन पड़ा। एक साल बाद, उन्होंने कलियम्मा से शादी कर ली किन्तु कुछ वर्षों के बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया।
नानू आसन ने अपने पिता और पत्नी की मौत के बाद एक विचरण करते हुए संन्यासी का जीवन अपना लिया। वह एक ‘परिव्राजक'( वह व्यक्ति जो सत्य की खोज में स्थान स्थान पर जाता है) बन गए । अपनी यात्रा के दौरान वह दो गुरुओं के संपर्क में आए, जिन्होंने उन पर गहरी छाप छोड़ी। उनमें से एक का नाम कुंजनपिल्लई था। वे चेट्टंबी स्वामी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। थिक्कड़अय्यावु अन्य गुरु थे। चेट्टंबी स्वामी एक महान विद्वान थे। उन्होंने नानू आसन की जन्मजात शक्तियों को पहचाना और नानू को संस्कृत में कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। थिक्कड़अय्यावु योग विज्ञान के विशारद थे। अपने गुरु से प्रेरित होकर नानू आसन ने ‘नव मंजरी’ (नौ छंदों की एक शृंखला) लिखी। उन्होंने अपनी कविताओं को चेट्टंबी स्वामी को समर्पित किया। अपने प्रवास के दौरान वह मारुथवामला स्थित पिल्लथदम गुफा पहुंचे जहां उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की और ध्यान और योग का अभ्यास किया ।1888 में, उन्होंने नदी से लाई गई चट्टान के एक टुकड़े को शिवमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो उसके बाद से अरुविप्पुरम शिव मंदिर के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर बन गया है। 15 मई 1903 को डॉ पद्मनाभनपल्पू ने नारायण गुरु की प्रेरणा से इस मंदिर में ‘श्री नारायण धर्म परिपालन योगम’ की स्थापना की। 1904 में उन्होने अपना केंद्र वरकला के पास शिवगिरी में स्थानांतरित कर दिया। जहां उन्होंने समाज के निम्न वर्ग के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और जहां वह उनकी जाति पर विचार किए बिना उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करते थे।उन्होंने वहां भी एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे 1912 तक शारदा मठ के नाम से जाना जाता था। उन्होंने त्रिशूर, कन्नूर, अंचुथेंगु, थालास्सेरी, कोझीकोड और मैंगलोर जैसे अन्य स्थानों में कई मंदिरों का निर्माण किया। प्रेम और मानवता के प्रसार की लंबी यात्रा के बाद वह सारदा मठ लौटे और यहीं पर उन्होंने 73 साल की उम्र में 20 सितंबर 1928 को अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया।
उनका योगदान
बचपन से ही वह जाति भेद और छुआछूत के प्रति गहन घृणा रखते थे और उन्होंने सदैव अन्याय का विरोध किया । ” जाति के बारे में मत पूछो, मत कहो और न हीं सोचो” उनका आदर्श वाक्य था । उनका पहला क्रांतिकारी कदम 1888 में अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का अभिषेक था। उन्होंने घोषणा की कि हर किसी को अपनी जाति या धर्म पर ध्यान दिये बिना भगवान की अनुभूति करने का अधिकार है ।
बाद के वर्षों में उन्होंने क्रांतिकारी बदलावों के साथ केरल के विभिन्न हिस्सों में कई मंदिरों की स्थापना की। शेरथलाई के कलावनकोड स्थित एक मंदिर में देवी-देवताओं के बजाय उन्होंने पूजा के लिए दर्पण स्थापित किया, जिससे सत्य का स्पष्टीकरण हो सके कि भगवान आपके अपने भीतर हैं और किसी को आंतरिक स्व के विकास से मोक्ष प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। त्रिवेंद्रम के पास मुरिककुंझा में एक अन्य मंदिर में, एक देवता के स्थान पर, एक उज्ज्वल प्रकाश पुंज को स्थापित किया गया जिसमे “सत्य, कर्तव्य, दयालुता, प्रेम” शब्दों का दृष्टिगोचर किया गया था। उनके मंदिर जाति या धर्म भेद के बिना सभी के लिए खुले थे।
उन्होंने समानता का पाठ पढ़ाया किन्तु साथ ही साथ यह भी अनुभव किया कि धर्मांतरण करने के लिए असमानताओं का अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए और इसलिए समाज में संघर्ष नहीं पैदा करना चाहिए । नारायण गुरु ने १९२३ में “बहस करने और जीतने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए और ज्ञात करने के लिए” के नारे के साथ एक अखिल क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया, , जो भारत में इस तरह का पहला आयोजन था । यह धर्मांतरण का मुकाबला करने का प्रयास था । 1925 में नारायण गुरु ने प्रसिद्ध वैकोम सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन किया, जिसने वैकोम में शिव मंदिर और केरल के सभी मंदिरों में निचली जाति के लोगों के प्रवेश की मांग की गयी थी। महात्मा गांधी ने इस दौरान केरल का दौरा कर वैकोम सत्याग्रह का समर्थन किया और शिवगिरी आश्रम में श्री नारायण गुरु से भेंट की और उन्होंने जाति और छुआछूत के मुद्दों पर उनके साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं कीं। इस अवसर पर गांधीजी ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि श्री नारायण गुरु जैसे सम्मानित ऋषि के दर्शन करना उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य था।
नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1922 में नारायण गुरु से मुलाकात की थी। गुरु के साथ अपनी ऊष्मित मुलाकात के बारे में टैगोर ने बाद में कहा: “मैंने विश्व के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया है किन्तु मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो आध्यात्मिक रूप से श्री नारायण गुरु के कद से बड़ा हो ।
उन्होंने स्वच्छता, शिक्षा को बढ़ावा देने, कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और तकनीकी प्रशिक्षण के आदर्शों के अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री नारायण गुरु के आद्यारोपदर्शनम (दर्शनमाला) के विचार ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताते हैं।
उनके दैवदशकम और अटमोपदेशसतकम के सिद्धांत कुछ ऐसे उदाहरण है जो इस बात की ओर संकेत करते है कि रहस्यवादी प्रतिबिंब और अंतर्दृष्टि सूक्ष्मता के विचार किस प्रकार से आधुनिक भौतिकी के क्षेत्र में हुई हाल ही में प्रगति से समानता रखते हैं।
नारायण गुरु संस्कृत के महान विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत और मलयालम दोनों में कई पुस्तकें लिखीं। उनकी लिखी ‘जाति मीमांसा’ (जाति का परीक्षण ) नामक पांच छंदों में एक कविता का बहुत महत्व है। यह संक्षेप में गुरु के जीवन दर्शन को प्रस्तुत करता है। पहला श्लोक संस्कृत में है। उन्होंने मलयालम, संस्कृत और तमिल भाषाओं में ४५ रचनाएँ प्रकाशित कीं, जिनमें आत्मोपदेशसतकम- सौ-श्लोकों की आध्यात्मिक कविता और दैवदसकम-दस छंदों में एक सार्वभौमिक प्रार्थना सम्मिलित है। उन्होंने तीन प्रमुख ग्रंथों, वल्लुवर के थिरुकुरल, ईशावस्य उपनिषद कनुदैयावल्लार के ओझिलओडुकम का भी अनुवाद किया। उन्होंने आदर्श एक जाति, एक धर्म, सभी के लिए एक ईश्वर (ओरूजाथी, ओरूमैथम, ओरूडीथम, मनुशुयुनु) के आदर्श का प्रचार किया जो केरल में एक कहावत के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। उन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन को सामाजिक समानता और सार्वभौमिक भाईचारे की अवधारणाओं से जोड़कर उनका व्यावहारिक निरूपण किया।
श्री नारायण गुरु जीवनी सिर्फ एक संत के जीवन की कहानी नहीं है अपितु यह सामाजिक बुराइयों और सामाजिक पुनरुत्थान के जागृति के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध का एक महाकाव्य है । गुरु को पता था कि अध्यात्म को लाखों भूखे लोगों को नहीं खिलाया जा सकता। उनका मानना था कि छुआछूत के अभिशाप से मुक्ति के अतिरिक्त वंचित और पिछड़े वर्ग को शिक्षा और धन की भी आवश्यकता है। उन्हें दूसरों की तरह सुधार करने के अवसरों की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि तीर्थयात्रा का लक्ष्य शिक्षा, स्वच्छता, ईश्वर के प्रति भक्ति, संगठन, कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना होना चाहिए। वह एक वास्तविक कर्मयोगी थे और उनका पूरा जीवन दबे-कुचले लोगो की बेहतरी के लिए समर्पित था। वे एक सहज कवि और मलयालम, तमिल और संस्कृत में महान विद्वान थे। वह इन भाषाओं में कई सुंदर और प्रेरणादायक रचनाओं के लेखक थे । उनके शब्दों और कामों ने एक क्रांति की चिंगारियों को प्रज्वलित किया जिसके कारण केरल के अपव्ययी समाज में उल्लेखनीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ । आदि शंकराचार्य के बाद भारत में सामाजिक सुधारों के लिए आगे आने वाले वह महानतम हिंदू सुधारकों में से एक थे ।